अपने भीतर के काले बन्दर को देखने की कमज़ोर कोशिश...दिल्ली-६
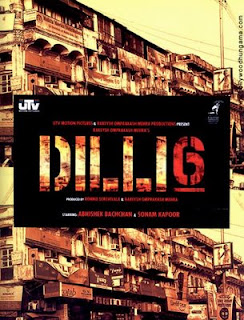
दिल्ली-६ कई मायनो में ख़ास फ़िल्म होते-होते रह जाती है.यह अक्सर होता है कि जब कोई निर्देशक एक बढ़िया फ़िल्म दे देता है तब उससे दर्शकों की उम्मीदें अधिक बढ़ जाती हैं.क्योंकि तब वह अपना एक दर्शक वर्ग बना चुका होता है.'रंग दे बसंती'से राकेश ने हिन्दी सिनेमा में २१वी सदी के यूथ की चिंता और सोच को एक रचनात्मक रूप देते हैं और लगभग स्तब्ध करते हैं.यही इस फ़िल्म को बड़ा कद देती है.इस फ़िल्म ने दिल्ली-६ के लिए पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि अब राकेश क्या देने जा रहे हैं.दिल्ली-६ का ताना-बाना ४ स्तरों पर तैयार करने के बावजूद भी राकेश फ़िल्म को संभाल नहीं पाये हैं.टुकडों-टुकडों में सभी को यह फ़िल्म पसंद आ सकती है या आई है,पर राकेश के निर्देशक कद के लिहाज़ से यह सतही होकर रह गई है.फ़िल्म का एक एंगल वहीदा रहमान के दिल्ली-६ से जुड़ता है जहाँ वह अपने अन्तिम दिनों के लिए अपनी मिटटी में आती है और साथ में उनका पोता अभिषेक बच्चन (रोशन)भी है.पर कुछेक घटनाओं के बाद दादी का यह कहना कि "अब तो यहाँ मरने का भी दिल नहीं करता.."वर्तमान राजनितिक-सामाजिक स्थितियों की ओर इशारा कर देता है.आख़िर दिल्ली-६ ही नहीं पूरे भारत के कंपोजिट कल्चर को 'अयोध्या,गोधरा,और मालेगाँव जैसी घटनाओं ने प्रभावित तो किया ही है और वह भी बड़े स्तर पर.दूसरा एंगल ओमपुरी-पवन मल्होत्रा के परिवारों,मुनीम जी-मुनीम की जवान बीवी और फोटोग्राफर ,मौलवी और कुछ मुसलमान किरदारों के साथ जुड़ता है.फ़िल्म के पहले हाफ में ये एंगल दिल्ली के कस्बाई कल्चर को ठीक-ठाक ढंग से दिखा जाती है और आप मुस्कराते हुए इंटरवल की देहरी पर आ पहुँचते हैं. सोनम कपूर और अभिषेक की केमेस्ट्री ठीक-ठाक लगी है.पर एक फ़िल्म को एक स्तर देने में स्क्रिप्ट का भी योगदान होता है जो अन्तिम तक दर्शकों को बांधता है,बस इसी की कमी अन्तिम के १५-२० मिनट्स में खल जाती है जब राकेश मेहरा फ़िल्म के ट्रीटमेंट के साथ रिस्क नहीं ले पाते और हीरो को जिंदा रख देते हैं.ऐसा शायद दर्शकों की डिमांड को ध्यान में रख कर किया गया है पर,यह समझ नही आता कि ये समझौता राकेश ओमप्रकाश मेहरा जैसे डाईरेक्टर को क्योंकर करना पडा.?बहरहाल,तीसरा एंगल रामलीला वाले प्रसंग का है जिसके दोहों और चौपाईयों के इर्द-गिर्द फ़िल्म की घटनाएं अपना आकार ले रही हैं.फ़िल्म के इस हिस्से में राकेश का कौशल दिखा है.शायद राम के रामराज्य का कोंसेप्ट निर्देशक के ध्यान में था ...तभी तो अन्तिम के दृश्यों में राकेश एक यूटोपियन समाज की रचना करते दिखे हैं..अतिशय प्रयोग भी कभी-कभी बुरा हो जाता है.'मसकली 'की मटकन ही फिम के अंत तक याद रह जाती है,यह रंग दे बसंती के निर्देशक की असफलता है.हिंदू-मुसलमानों के आपसी बैर और उसमें नेता-साधु गठबंधन तथा काले बन्दर के त्रियोग से हम सब के भीतर झाँकने की पुरजोर कोशिश है.फ़िल्म के दो किरदार प्रभावित करते हैं-पहला वह जो आइना लिए दिल्ली-६(पता नहीं चांदनी चौक का माहौल रचने के बाद निर्देशक अपने चरित्रों के मुहँ से बार-बार 'हम दिल्ली-६ वाले..जुमला क्यों कहला रहा है.भला कोई अपने पिन कोड से अपने ट्रेडिशन को बताता है क्या ) के मुख्य किरदारों के चेहरों के आगे कर देता है,यह कैरेक्टर कम उपस्थिति के बावजूद फ़िल्म के बाद भी याद रहता है.किसी ने सही ही लिखा है कि "आईना देखने से डरता है आदमी/कहीं उसकी ख़ुद से मुलाकात न हो जाए" -पर,जब फ़िल्म में नायक को इस आईने को दिखाए जाने की व्याख्या करते दिखाया जाता है तो दर्शक एक बार फ़िर कोफ्त से भर जाता है. फ़िल्म देखने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को इसकी व्याख्या गैर-जरुरी लगेगी.-दूसरा किरदार 'जलेबी'(दिव्या दत्ता) का है,जिसमें इस उदार,संस्कृत,सामाजिक सद्भाव के अग्रदूत भारतीय समाज का फर्जी चेहरा बेनकाब होता है.दिल्ली-६ के बढ़ते बच्चों को 'जलेबी'जवान करती है,कोतवाल के जवान धड़ की मांसल जरुरत का साधन है और सबका कूड़ा साफ़ करने के बावजूद मन्दिर के भीतर आने का अधिकार नहीं रखती.राकेश ओमप्रकाश ने बढ़िया कलाकारों का चयन किया है पर २ घंटे १८ मिनट की फ़िल्म में कुछ तो अंत तक अंट नहीं पाये.रघुवीर यादव जैसा कलाकार रामलीला ही गाता रह जाता है और आप यदि ध्यान से ना देखे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह रामायण गा कौन रहा है.
समस्या फ़िल्म के पूरे ट्रीटमेंट को लेकर नहीं जनमती बल्कि अंत के २० मिनटों को लेकर है.रंग दे...में फ़िल्म के वह सारे किरदार जो पहले हाफ में 'मस्ती की पाठशाला ...'-को ही अपना लाईफ मंत्रा बताते हैं वह कैसे इस पूरे सिस्टम से युवा असंतोष की पहचान बन जाते हैं और शहीद हो जाते हैं.इसी ट्रीटमेंट ने रंग दे...को एक क्लासिक फ़िल्म का दर्जा दिया और हमारी अपेक्षाएं 'दिल्ली-६'से बढ़ गई.पर,अफ़सोस इस बार राकेश रिस्क नहीं ले पाये..फ़िल्म का ट्रेडिशनल एंड रखने के बजाये ओपन एंड ही रहता और रोशन(नायक) का किरदार उस दंगे की बलि चढ़ जाता तो मज़ा कुछ और ही होता.क्योंकि आज जिस तरह का परिवेश हमारे आकाओं (तथाकथित)ने रच दिया है उसमें ह्रदय-परिवर्तन की बाद थोडी अटपटी लगती है,एक दूसरे को मारने कूटने पर आमादा भीड़ यदि एक भाषण से रास्ते आ जाए तो हमारे आसपास ऐसे सैकडों भाषणबाजिये हैं.हिंदू धर्म में लाईफ को सर्कुलर माना गया है कि-'जीवन का अंत नहीं होता'-इसी कारण हमारे नाटकों में सुखांत का प्रावधान है और इसीसे सिनेमा में भी यह आया पर क्या हमारा सिनेमा ऐसा ही रहा है..नहीं .फ़िर भी ...राकेश से ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी.फ़िल्म चल रही है ,हिट भी हो जायेगी पर यह एक बढ़िया निर्देशक के सतही काम का नमूना है.. काश,अपने भीतर छुपे इस काले बन्दर को हम सभी देख लेतें .....तब शायद मसकली और बढ़िया से मटक पाती.
समस्या फ़िल्म के पूरे ट्रीटमेंट को लेकर नहीं जनमती बल्कि अंत के २० मिनटों को लेकर है.रंग दे...में फ़िल्म के वह सारे किरदार जो पहले हाफ में 'मस्ती की पाठशाला ...'-को ही अपना लाईफ मंत्रा बताते हैं वह कैसे इस पूरे सिस्टम से युवा असंतोष की पहचान बन जाते हैं और शहीद हो जाते हैं.इसी ट्रीटमेंट ने रंग दे...को एक क्लासिक फ़िल्म का दर्जा दिया और हमारी अपेक्षाएं 'दिल्ली-६'से बढ़ गई.पर,अफ़सोस इस बार राकेश रिस्क नहीं ले पाये..फ़िल्म का ट्रेडिशनल एंड रखने के बजाये ओपन एंड ही रहता और रोशन(नायक) का किरदार उस दंगे की बलि चढ़ जाता तो मज़ा कुछ और ही होता.क्योंकि आज जिस तरह का परिवेश हमारे आकाओं (तथाकथित)ने रच दिया है उसमें ह्रदय-परिवर्तन की बाद थोडी अटपटी लगती है,एक दूसरे को मारने कूटने पर आमादा भीड़ यदि एक भाषण से रास्ते आ जाए तो हमारे आसपास ऐसे सैकडों भाषणबाजिये हैं.हिंदू धर्म में लाईफ को सर्कुलर माना गया है कि-'जीवन का अंत नहीं होता'-इसी कारण हमारे नाटकों में सुखांत का प्रावधान है और इसीसे सिनेमा में भी यह आया पर क्या हमारा सिनेमा ऐसा ही रहा है..नहीं .फ़िर भी ...राकेश से ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी.फ़िल्म चल रही है ,हिट भी हो जायेगी पर यह एक बढ़िया निर्देशक के सतही काम का नमूना है.. काश,अपने भीतर छुपे इस काले बन्दर को हम सभी देख लेतें .....तब शायद मसकली और बढ़िया से मटक पाती.
Comments
अज्ञेय को याद करते हुए...
"जैसे बर्तन को अधिक घिसने से छूट जाता है उसका मुलम्मा."